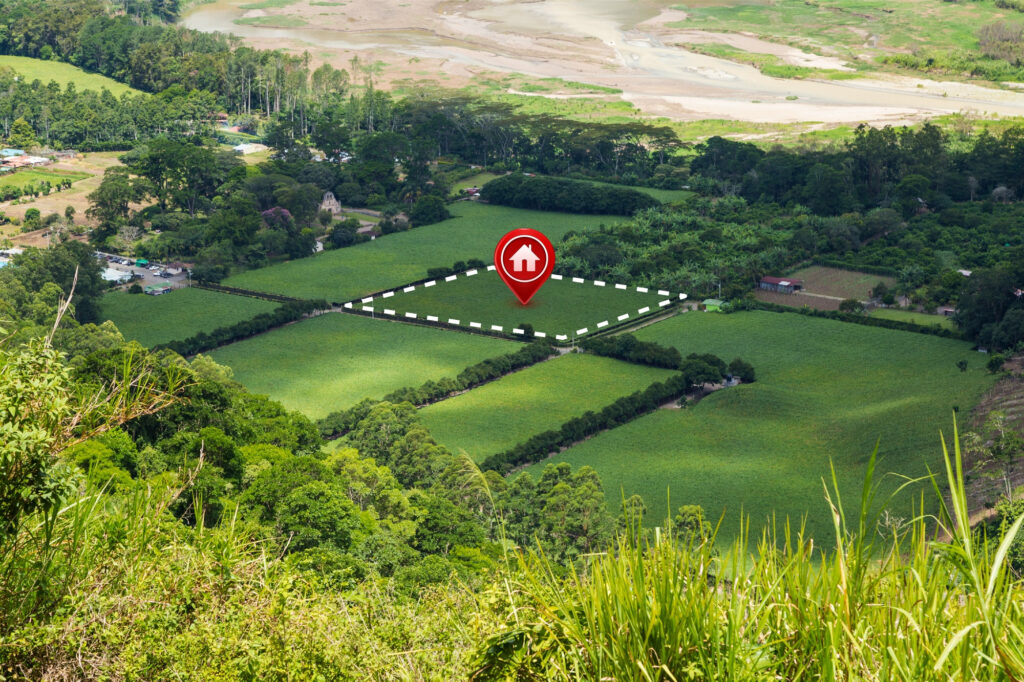NCERT Solutions for Class 10th:
पाठ 1- संसाधन और विकास भूगोल
1. पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर:
(घ) अति पशुधारण
कारण: अति पशुधारण से भूमि की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है और भूमि की उपजाऊ शक्ति घटती है, यह भूमि विनीकरण का एक बड़ा कारण है।
2. सीढ़ीदार (सोपानी) खेती किस प्रांत में की जाती है?
उत्तर:
(घ) उत्तराखण्ड
कारण: उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहाँ भूमि ढलानदार होती है। इसलिए वहाँ मृदा अपरदन को रोकने और खेती योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए सीढ़ीदार खेती की जाती है।
3. काली मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है?
उत्तर:
(ग) महाराष्ट्र
कारण: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, जिसे "रेगूर मृदा" भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
4. तीन राज्यों के नाम जहाँ काली मृदा पाई जाती है, और उस पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल:
उत्तर:
-
राज्य: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात
-
मुख्य फसल: कपास (काली मृदा को 'कपास की मृदा' भी कहते हैं)
5. पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा, और उसकी तीन विशेषताएँ:
उत्तर:
-
मृदा का प्रकार: जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil)
-
तीन विशेषताएँ:
-
यह बहुत उपजाऊ होती है।
-
इसमें पोटाश, फॉस्फोरस, चूना आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं।
-
इसमें धान, गन्ना, गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
-
6. भूमि संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए?
उत्तर: भूमि संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए
-
वृक्षारोपण करना
-
सीढ़ीदार खेती को बढ़ावा देना
-
वर्षा जल संचयन
-
अधिक चराई पर रोक
-
जैविक खाद का प्रयोग
-
मृदा परीक्षण कर उर्वरकों का उपयोग
7. भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें:
उत्तर:
भारत में भूमि का उपयोग मुख्यतः निम्न वर्गों में होता है:
-
कृषि योग्य भूमि
-
वनों के अंतर्गत भूमि
-
चारागाह और स्थायी चराई भूमि
-
बंजर और अनुपजाऊ भूमि
-
आवास, उद्योग और सड़कों हेतु उपयोग
8. वर्ष 1960-61 से वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि क्यों नहीं हुई?
उत्तर:
-
बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि और आवास हेतु वनों की कटाई
-
अवैध वनों की कटाई
-
औद्योगीकरण और शहरीकरण
-
वनों की पुनर्स्थापना में सरकार की धीमी गति
9. प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है?
उत्तर:
-
उद्योगों का विस्तार: जल, खनिज, वन जैसे संसाधनों की अत्यधिक खपत
-
शहरीकरण: भूमि और जल का अधिक प्रयोग
-
बिजली और परिवहन: कोयला, पेट्रोलियम आदि का अत्यधिक दोहन
-
पर्यटन और निर्माण: प्राकृतिक स्थानों का दोहन
अत्ति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. राष्ट्रीय वन नीति (1952) के अनुसार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अन्तर्गत होना चाहिए।
उत्तर
33%
प्रश्न 2. प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं ? इसके कोई दो उदाहरणलिखिए।
उत्तर
वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।
उदाहरण – जल, वन इत्यादि।
प्रश्न 3. परती भूमि से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर
यह कृषि योग्य भूमि है जिस पर एक या इससे अधिक वर्ष तक खेती नहीं की गई है। यही खाली छोड़ी गई भूमि परती भूमि कहलाती है।
प्रश्न 4. आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ कितने प्रकार की होती हैं ?
उत्तर
आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ दो प्रकार की हैं :
- पुराना जलोढ़ (बांगर)
- नया जलोढ़ (खादर)
प्रश्न 4. उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधनों के नाम लिखें।
उत्तर
दो संसाधनों के नाम:
- जैव संसाधन
- अजैव संसाधन
प्रश्न 5. नवीनीकरण संसाधन क्या है ? परिभाषा दीजिए।
उत्तर
वे संसाधन जिन्हें बार-बार पुनर्जीवित या पुन: उपयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं।
उदाहरण – जल, मिट्टी आदि।
प्रश्न 6. राजस्थान में किन ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत है?
उत्तर
पवन और सौर ऊर्जा।
प्रश्न 7. भारत में अनेक प्रकार की मृदाए होने का क्या कारण है?
उत्तर
भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू-आकृतिया, जलवायु के कारण अनेक मृदाए विकसित हुई हैं।
प्रश्न 8. मृदा अपरदन क्या हैं?
उत्तर
मृदा के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं।
प्रश्न 9. लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता हैं?
उत्तर
लौह ऑक्साइड के कारण।
प्रश्न 10. तीन राज्यों के नाम बताएँ काली मृदा पाई जाती है | इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है ?
उत्तर
महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्यप्रदेश में काली मृदा पायी जाती है। इस पर ज्यादातर कपास की खेती की जाती है।